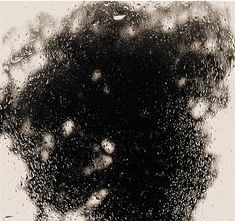हर युवा कवि अपनी रचना और विचार-प्रक्रिया में ख़ुद को पूर्वज कवियों से साझा करता है। मेरे लिए पूर्वज कवियों का स्मरण एक आवेगपूर्ण घटना है – यूँ किसी भी समय में किसी का कवि हो जाना भी एक घटना ही है – कुछ ऐसी घटना, जिसे कबीर ने एक अवान्तर ईश-प्रसंग में `घट-घट में पंछी बोलता´ कहकर व्यक्त किया है। मेरे थोड़े-से इस कवि-जीवन में कितनी तो पूर्वज कविता ऐसी है, जो घट-घट में बोलती है। उसमें अमीर ख़ुसरो हैं, कबीर हैं, नज़ीर हैं, मीर हैं, ग़ालिब हैं, निराला हैं, फ़ैज़ हैं, नागार्जुन हैं, मुक्तिबोध हैं, धूमिल हैं – और निश्चित रूप से एक बहुत बड़े स्पेस के साथ शमशेर हैं। बहुत उत्सुकता से मैं देखता हूँ कि हमारे अग्रजों में आलोक धन्वा, वीरेन डंगवाल, मनमोहन और मंगलेश डबराल हैं, जो शमशेर के साथ अपनी कविता में बहुत कुछ साझा करते हैं। यहां मैं शमशेर की कही-लिखी कुछ बातों के सहारे अपनी इस साझेदारी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा –
कला का संघर्ष समाज के संघर्षों से एकदम कोई अलग चीज़ नहीं हो सकती (१)
आज की कविता में, ख़ासकर नए लोगों के बीच कला या कलावाद एक बड़ी बहस का मुद्दा है। उदाहरण के लिए युवा कवियों में गिरिराज किराडू और किसी हद तक व्योमेश शुक्ल या उनकी कविता को लोग कलावादी कहते हैं और ऐसा कहते हुए वे अज्ञेय और अशोक वाजपेयी को तो याद रखते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शमशेर को भूल जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि जितनी कला शमशेर में है, उतनी अज्ञेय या उनके परवर्ती अलम्बरदारों में होगी – पर शमशेर की कला का संघर्ष, जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया है, समाज का संघर्ष है। यहां एक बात यह भी उठ सकती है कि ठीक है कथ्य आपका समाज का है, किन्तु उसे कहने का शिल्प इतना कलापूर्ण है कि वह जिस समाज का है, वही उसे समझ नहीं पाता। मैं कहना चाहता हूँ कवि का कथ्य हमेशा ही स्थूल सामाजिक आशयों का कथ्य नहीं होता, उस पर सूक्ष्मतम को गहने की जिम्मेदारी भी होती है। दरअसल भीतरी, गूढ़ और जटिल संरचनाओं किंवा कलाओं से ही बाहर का स्थूल और प्रकट रूप अस्तित्व में आता है- यह सिद्धान्त विज्ञान से लेकर समाज और साहित्य तक एक जैसा लागू होता है। फिर सवाल यह है कि कला कहते किसे हैं? यहां भी शमशेर ही साथ देते हैं –
आज की कला का असली भेद और गुण लोक-कलाकारों के पास है, जो जनान्दोलनों में हिस्सा ले रहें हैं……. हम-आप ही अगर अपने दिल और नज़र का दायरा तंग न कर लें तो देख सकेंगे कि हम सबकी मिली-जुली ज़िन्दगी में कला के रूपों का ख़ज़ाना हर तरह बेहिसाब बिखरा चला गया है….अब यह हम पर है, ख़ास तौर से कवियों पर, कि हम अपने सामने और चारों ओर की इस अनन्त और अपार लीला को कितना अपने अन्दर बुला सकते हैं। (२)
यहां बात न सिर्फ़ लोक-कलाकारों की हो रही है, बल्कि उन जनान्दोलनों की भी हो रही है, जिनमें वे भागीदार होते हैं। कला का बेहद निकट और आत्मीय सम्पर्क `जन´ से है। बात को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं `जनवादी कला´ यानी कला जो जन के हित में हो, उसके संघर्षों को स्वर देती हो, भले कभी बहुत पास और कभी कुछ दूर से देती हो, पर देती हो। तो इस तरह बरास्ता शमशेर मेरे लिए हर उस तरह की कला सर-माथे पर है, जिसका मूल तत्व जन है। शमशेर की कला का सबसे सार्थक प्रभाव किसी पर देखना हो तो आलोक धन्वा का अकेला संकलन `दुनिया रोज़ बनती है´ को पढ़ लेना चाहिए। उनके बिम्ब उतने ही हल्के-हवादार, धरती-आकाश के कोमल रंगों से भरे, भीतर वैसी ही आग-वैसे ही वास्तविक और समूचे जीवन-राग से रचे हैं, जैसे शमशेर के यहां है। अपने नव्यतम संग्रह `स्याही ताल´ के नाम से ही मानो वीरेन डंगवाल शमशेर का सुमिरन कर लेते हैं और फिर अन्दर आलोक धन्वा को समर्पित एक कविता की पंक्ति ` एक बादल जो दरअसल एक नम दाढ़ी था´ में शमशेर से वीरेन डंगवाल तक की पूरी परम्परा एकमेक हो जाती है, जिससे अगर सीखना चाहे, तो हमारी पीढ़ी बहुत कुछ ऐसा सीख सकती है, जिसे एक शब्द में `कला´ कहना चाहिए । शमशेर को निरन्तर पढ़ने से मिली इस समझ के सहारे मैं कह सकता हूँ कि कला का जो प्रश्न औरों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, वह मेरे लिए दो दूनी चार की तरह सरल होकर सामने आता है। मुझ समेत सभी को चिन्ता करनी चाहिए कि इक्कीसवीं सदी में हमारे लिए `लोक-कलाकार´ और `जनान्दोलन´ जैसे क़ीमती शब्दों के अब क्या मायने हैं। आज की कविता के सामने सबसे बड़े प्रश्न यही हैं कि हमारा `जन´ कौन है? कैसा है? कहां है? उसके क्या हक़-हुक़ूक हैं? और इन सबसे बढ़कर यह कि हम ख़ुद क्या ठीक वही `जन´ नहीं हैं? हमारी तंगदिली हमें एक दिन कहीं का नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि हमने अपने जीवन की सीमाएं तय कर ली हैं और साथ ही लिखी-पढ़ी जा रही कविता की भी। हमें जल्दी, किसी तरह अपने भीतर को बाहर प्रदर्शित कर देने की है, बाहर को भीतर बुलाने के प्रयास कमतर होते गए हैं। कविता लिखना एक नितान्त बौद्धिक कृत्य होता गया है। इस अंधेरे में मैं टटोलता हुआ चलता हूँ तो शमशेर किसी अनन्त से मेरी ओर बढ़ा हाथ हो जाते हैं। पुरखों के बारे में बहुत महत्वाकांक्षी होकर कहूँ तो मुझे बुद्धि मुक्तिबोध की चाहिए और हृदय नागार्जुन का पर हाथ हमेशा शमशेर का चाहिए, जिसे थामकर पिछले पचास साल की कविता की जटिलता में राह खोजना और अपनी राह बनाना, दोनों ही कुछ आसान हो पाते हैं। कविता में कला की सच्ची शिनाख़्त करना चाहूँ तो शमशेर के ठीक अगल-बगल खड़े आलोक धन्वा, वीरेन डंगवाल, मनमोहन और मंगलेश डबराल का मेरे मन में खिंचा यह ग्रुपफोटोग्राफ़ आश्वस्त करता है कि कला और कविता के बारे में मेरी ये धारणाएं आभासी नहीं, वास्तविक हैं। और वास्तविक मेरे लिए एक बड़ा शब्द है – महान, अनन्त और अपार।
जब `वास्तविक´ कहता हूँ तो यह विचार के बीहड़ में उतरना होता है। जीने और जीते रहने के लिए वैज्ञानिक जीवनदृष्टि की एक टीसभरी खोज। जो है, वही वास्तविकता नहीं है- जो होना चाहिए, वह भी वास्तविकता है। वास्तविकता क्या है, क्या होनी चाहिए का एक जटिल संसार मेरे सामने खुलता है। स्मृति और स्वप्न के बीच कहीं एक वास्तविकता है, जो मेरी है। मिट्टी की परतों में राह तलाशते ख़तरों से घिरे किसी नन्हें जीव की-सी उद्धिग्नता और छटपटाहट। मेरे चारों ओर परभक्षी विचारधाराओं के झपट्टे और कितना तो लोभ, जो जीवन को सरल बनाता दीखता है, पर जीवन कभी सरल नहीं होता। अपने जीवन को खोजने के लिए एक वैज्ञानिक आधार की तलाश हर कवि की तलाश है। शमशेर ने अज्ञेय के दूसरा सप्तक के अपने हिस्से के वक्तव्य में अगर यह घोषणा की है कि मेरे लिए यह वैज्ञानिक आधार मार्क्सवाद है (३) तो मेरे लिए इसका एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। शमशेर की पुरानी कविता `समय साम्यवादी´ ने १७ -१८ की उम्र में मेरे भीतर जैसे एक रूमान को जन्म दिया था। दीवारों पर आइसा का प्रतीक चिन्ह `तीन सितारों की छांव तले तना हुआ मुक्का´ बनाते हुए दिल फड़फड़ाता हुआ बार-बार यही दुहराता था –
वाम वाम वाम दिशा
समय-साम्यवादी
पृष्ठभूमि का विरोध
अंधकारलीन
व्यक्ति – कुहाSस्पष्ट हृदय-भार आज, हीन
हीन भाव, हीन भाव, हीन भाव…..
मध्यवर्ग का समाज, दीन (४)
शमशेर की कविता की बदौलत ज़िन्दगी में आया यह रूमान बाद में मुक्तिबोध को पढ़ते हुए पका। प्रेम बना। जीवन में बसा। मेरी दुनिया कई सही-ग़लत काम करते या उनका भागीदार बनते, कहीं न कहीं उसी रूमान से संचालित होती रही है। एक कवि आपकी जीवनचर्या में घुस सकता है, उसे बदल सकता है, इस चीज़ को मेरे लिए शमशेर की कविता ने सम्भव कर दिखाया है। और यह तो महज विचार की बात है, सौन्दर्यबोध, शरीरबोध और बिम्बबोध के तो पहलू अनेक हैं।
दो चार अलग-अलग भाषाओं के अलग-अलग मिज़ाज की, और उनकी अलग-अलग तरह की रंगीनियों और गहराइयों की जानकारी हमें जितना ज़्यादा होगी उतना ही हम फैले हुए जीवन और उसको झलकाने वाली कला के अन्दर सौन्दर्य की पहचान और सौन्दर्य की असली कीमत की जानकारी बढ़ा सकेंगे। (५)
शमशेर की इस सीख के आगे कभी-कभी बहुत शर्मिन्दग़ी महसूस करता हूँ। इस मामले में अनपढ़ ही रहा। अंग्रेज़ी का कामचलाऊ (पढ़ पाने और अंग्रेज़ी से कविताओं का हिन्दी अनुवाद कर पाने भर) ज्ञान अर्जित कर पाया, हालांकि उसने भी दिमाग़ में कई खिड़कियां खोल दी हैं। उर्दू की लिपि नहीं जानता लेकिन देवनागरी में उपलब्ध नज़ीर, मीर, ग़ालिब और फ़ैज़ ने भीतर कुछ तो जोड़ा ही है, इतना मैं जानता हूँ। मेरे लिए भाषा नहीं, बोलियों के स्तर पर यह ज़रूर सम्भव हुआ है। बुन्देलखण्डी, गढ़वाली और कुमाऊंनी बोलियों ने मेरी ज़िन्दग़ी में वह किया है, जिसे युवा कवि-आलोचक व्योमेश शुक्ल कविता में मेरी पहाड़ी-पठारी-मैदानी नागरिकता कहता है। लोक-कलाकारों की बात शमशेर ने बहुत ज़ोर देकर कही है और जन-आन्दोलनों की भी। मेरी पहाड़ी बोलियों में मैंने इन दोनों का लम्बा और अन्तरंग सानिध्य प्राप्त किया है। इससे मेरी कविता प्रभावित हुई है और उसमें जीवन का फैलाव बढ़ा है। उसके ठस और सूखे शिल्प में पानीदार प्राणवायु के लिए कुछ जगह बन सकी है।
शमशेर की बात हो, याद हो, तो मुक्तिबोध स्वाभाविक रूप से वहां हमेशा ही मौजूद होंगे। `चांद का मुंह टेढ़ा है´ से ही मुक्तिबोध की कविता किसी भी युवा के लिए गहरे आश्चर्य, वैचारिक-बौद्धिक आकर्षण, सामाजिक-राजनीतिक हादसों और जीवन की जटिलताओं का एक गूढ़बंध साबित होती है। मगर कितनी ख़ुशी की बात है कि वहां भी किसी कुशल प्राध्यापक और पथप्रदर्शक की तरह शमशेर मौजूद हैं। उनके पास वे चाबियां हैं, जिनकी ज़रूरत मुक्तिबोध को पढ़ते हुए हमें महसूस होती है। बहुत बाद में चन्द्रकान्त देवताले ने मालवा के देहातों में मुक्तिबोध का लैण्डस्केप मुझे दिखाया तो लगा जो सफ़र शमशेर के साथ शुरू हुआ था, वो आज देवताले जी के साथ पूरा हुआ। शमशेर ने बाद में भी मुक्तिबोध पर बहुत कुछ लिखा। उनके इधर-उधर बिखरे कुछ संस्मरणों, लेखों और साक्षात्कारों में कई बातें ऐसी हैं, जो मुक्तिबोध को समझने की नई दृष्टि प्रदान करती हैं।
मुक्तिबोध के साथ मेरी समस्या होती है(अकसर ही पाठकों को होती है, मैं भी एक साधारण ही पाठक हूँ) अव्वल तो पढ़ने की! (ईमानदारी की बात) रचना की दीर्घकाय विराटता हताश करती है। ए ग्रिम रियलिटी( अन्दर-बाहर सब ओर से। वस्तु और शिल्परूप और अन्तरात्मा, रचना-प्रक्रिया और पाठक की प्राथमिक प्रतिक्रिया सबमें एक अजब ग्रिमनेस, मैं बचकर कहां जा सकता हूँ। घिर ही जाता हूँ, फंस ही जाता हूँ …..निस्तार नहीं, तभी `मुक्ति´ है — `मुक्ति-बोध´ हैं।
दूसरी समस्या होती है समझने की। होती थी ….कहना चाहिए। क्योंकि पढ़ लेने, और अर्थ और भाव-व्यंजनाएं हृदयंगम कर लेने के बाद कविता हृदय पर, चेतना पर हावी हो जाती है। आप मुक्तिबोध के चित्रों के पैटर्न समझ लेने के बाद उन्हें उम्र भर नहीं भूल सकते। (६)
तो इस तरह पढ़ा जाना चाहिए मुक्तिबोध को। शमशेर सिर्फ़ दीर्घकाय कहकर नहीं रह पाए, उन्हें उसके साथ विराटता भी कहना पढ़ा। व्याकरण के हिसाब से ग़लत पर मुक्तिबोध की कविता को समझने के अपने विशिष्ट व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल सही। कविताओं में जीवन और उसकी ऐतिहासिक-सामाजिक-राजनीतिक-वैज्ञानिक-वैचारिक स्थितियों के उस रचाव को, जिसे मुक्तिबोध आश्चर्यजनक ढंग से सम्भव करते हैं, बिना इतने विशेषणों के नहीं समझा जा सकता। मैंने पहले भी कहा कि `वास्तविकता´ मेरे लिए एक बड़ा शब्द है – महान, अनन्त और अपार। यह संस्कार मुक्तिबोध से ही आया है। और देखिए शमशेर मुक्तिबोध में मौजूद उस वास्तविकता को ग्रिम कहते हैं यानी – क्रूर, निर्दय, भयानक…. तभी मैं समझ पाता हूँ कि वास्तविकता वह भी है जो नहीं होनी चाहिए या किंचित उलटबांसित फेरबदल के साथ कहूँ तो वह भी, जैसी होनी चाहिए। और ग्रिमनेस भी महज ग्रिमनेस नहीं है – ‘अजब ग्रिमनेस’ है। हमारे बदलते जीवन और समाज में कितना अर्थपूर्ण और अपार होता जा रहा है यह एक शब्द – अजब! यहां सिर्फ़ हैरत नहीं, समूची मानवजाति की विडम्बनाओं-विसंगतियों का भूत है और भविष्य भी। वर्तमान के तो कहने ही क्या! और आगे यह कि निस्तार में मुक्ति नहीं – निस्तार नहीं है, तभी मुक्ति है और हमारे प्यारे मुक्तिबोध भी। यह जीवन का फ़लसफ़ा ख़ुद को साधारण कहते हुए शमशेर कितनी सरलता से समझा देते हैं। सीधा समीकरण यह है कि जो जीवन का फ़लसफ़ा है, वही कविता का भी। भाव-व्यंजनाओं को समझने की बात तो महज मुक्तिबोध पर नहीं, समूची कविता पर लागू होती है, जिसमें सबसे पहले ख़ुद शमशेर की कविता आएगी। चित्र पैटर्न ख़ुद शमशेर के देखिए – क्या कविता के हम सरीखे कार्यकर्ता उन्हें उम्र भर भुला पायेंगे….
निम्नमध्यवर्ग का शिक्षित व्यक्ति, अजब-सी सूली पर लटका रहता है और फिर भी ज़िन्दा रहता है, नरक में जाने के लिए, और अपने परिवार के साथ नरक ही भोगता है। (७)
मुक्तिबोध के सन्दर्भ में कही यह बात आज की भूमण्डलीकृत उत्तर बल्कि उत्तरोत्तरआधुनिक दुनिया और इसके निकटतम इतिहास में हम जैसों की सामूहिक जीवनगाथा बन जाती है। इसे सोचते और यहां लिखते हुए मेरे भीतर के मनुष्य और कवि का आकार मानो कहीं एकदम से टूटता, तो कहीं जुड़ता भी है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे पुरखे मिले हैं जो अपने बाद भी क़दम-क़दम पर हमारे सामाजिक-राजनीतिक जीवन और कविता में हमारा साथ देते हैं।
मुक्तिबोध का वास्तविक मूल्यांकन अगली, याने अब आगे की पीढ़ी निश्चय ही करेगी, क्योंकि उसकी करूण अनुभूतियों को, उसकी व्यर्थता और खोखलेपन को पूरी शक्ति के साथ मुक्तिबोध ने ही व्यक्त किया है। इस पीढ़ी के लिए शायद यही अपना ख़ास महान कवि हो। (8)
शमशेर ने कविता और कवियों के बहाने अपने समय को इस क़दर पहचाना है कि बाद के घटनाक्रम की तस्वीर भी वे हमारे लिए बना गए। हमारी व्यर्थता, हमारा खोखलापन, हमारी करूण अनुभूतियां, हमारे मुक्तिबोध और हमारे शमशेर ! सुन रहे हो मेरे हमउम्र कवि- साथियों? सुनो! सुनो, क्योंकि यही सुनने की बात है आज, और गुनने की भी। पुरखों की स्मृतियां जब इस तरह विकल हो पुकारती हैं तो हमारा वर्तमान और भविष्य गूंजता है उनमें।
उस महान मानवीय गूँज को मेरी पूरी पीढ़ी की ओर से मेरा सलाम, जिसमें हमारे अक्स झलकते हैं। और अगर नहीं झलकते तो हम कवि होने के क़ाबिल नहीं, न ही मनुष्य होने के!
———————————————————-
१. दूसरा सप्तक, प्रथम संस्करण, पृ0 ८५
२. वही, पृ0 वही
३. वही, पृ0 ८८
४. वही, पृ0 ११३
५. वही, पृ0 ८७
६. एक बिलकुल पर्सनल एसे, साक्षात्कार, अगस्त-नवम्बर, १९८६, पृ0 ७१
७. वही, पृ0 ७०
८. वही, पृ0 ७१